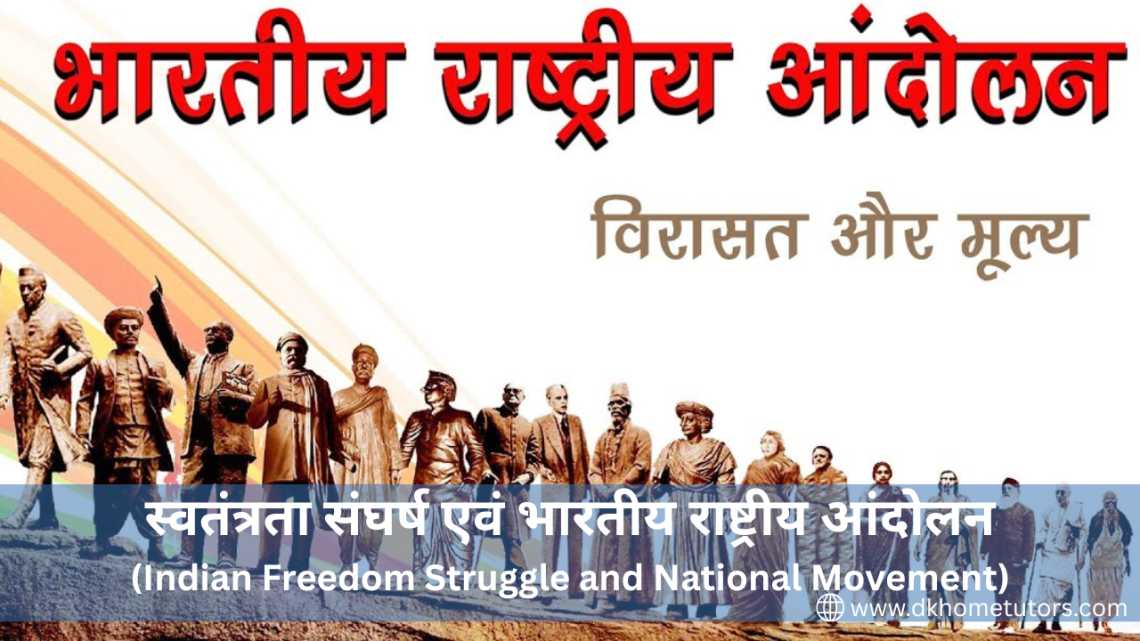भारत का स्वतंत्रता संघर्ष विश्व इतिहास के सबसे प्रेरणादायक और संघर्षपूर्ण आंदोलनों में से एक रहा है। यह केवल विदेशी शासन से मुक्ति का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह भारतीय समाज के पुनर्जागरण, एकता, समानता, और आत्म-सम्मान की भावना का प्रतीक था। इस संघर्ष ने भारतीयों को राष्ट्रीय चेतना, आत्मनिर्भरता, और लोकतांत्रिक मूल्यों की दिशा में अग्रसर किया। आइए, इस महान यात्रा को चरणबद्ध रूप से समझें।(Home Tutors Service)
1. ब्रिटिश शासन की स्थापना और शोषण की नीति
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 की प्लासी की लड़ाई में सिराज-उद-दौला को हराकर बंगाल पर अधिकार किया। इसके बाद 1764 की बक्सर की लड़ाई ने ब्रिटिशों की स्थिति को और मजबूत किया। कंपनी ने व्यापार के नाम पर भारत के राजनीतिक और आर्थिक तंत्र पर कब्जा कर लिया।
ब्रिटिश शासन ने भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया, किसानों पर अत्यधिक कर लगाए, और भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ब्रिटिश हितों के अनुसार ढाल दिया। इस आर्थिक शोषण ने जन-आक्रोश को जन्म दिया।
2. 1857 की क्रांति – प्रथम स्वतंत्रता संग्राम
1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पहली ज्वाला था। इसे “भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम” कहा जाता है।
इस विद्रोह के मुख्य कारण थे —
- सैनिक असंतोष (कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग)
- राजनीतिक असंतोष (लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति)
- आर्थिक शोषण और सामाजिक असमानता
इस आंदोलन का नेतृत्व मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, बेगम हजरत महल जैसे महान वीरों ने किया। यद्यपि यह क्रांति असफल रही, परंतु इसने भारतीय जनता में स्वतंत्रता की चेतना जगा दी।
3. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन (1885)
1857 के बाद भारतीय समाज में बौद्धिक और राजनीतिक जागृति का दौर शुरू हुआ। 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय नेताओं के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की।
कांग्रेस ने प्रारंभ में संविधानिक सुधारों और शांतिपूर्ण विरोध की नीति अपनाई।
इस दौर को “मॉडरेट युग” कहा गया, जिसमें दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोजशाह मेहता जैसे नेताओं ने कार्य किया।
4. उग्रवाद का उदय (1905-1919)
1905 में बंगाल विभाजन के बाद भारतीय राजनीति में उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ।
बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने “स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है” का नारा दिया।
इस काल में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई।
स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और ब्रिटिश वस्त्रों के बहिष्कार ने आर्थिक राष्ट्रवाद की नींव रखी।
5. गांधी युग का आरंभ (1915-1947)
महात्मा गांधी का भारत आगमन (1915) स्वतंत्रता आंदोलन का निर्णायक मोड़ था। उन्होंने सत्य, अहिंसा, और सत्याग्रह को राजनीतिक संघर्ष का आधार बनाया।
गांधीजी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जनता के बीच पहुंचाया और उसे एक जन-आंदोलन बना दिया।
(i) असहयोग आंदोलन (1920-22)
जलियांवाला बाग हत्याकांड (1919) और रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधीजी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया।
लोगों ने सरकारी पद, विद्यालय, और वस्त्रों का बहिष्कार किया।
हालाँकि चौरी-चौरा कांड के बाद यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया, परंतु इसने भारतीय राजनीति को नया आयाम दिया।
(ii) सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930)
1930 में गांधीजी ने दांडी यात्रा के माध्यम से नमक कानून का विरोध किया।
देशभर में ब्रिटिश शासन के प्रति असहयोग और अहिंसक विरोध की लहर उठी।
यह आंदोलन भारतीयों में आत्मबल और एकता का प्रतीक बना।
(iii) भारत छोड़ो आंदोलन (1942)
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में गांधीजी ने “अंग्रेज़ों भारत छोड़ो” का नारा दिया।
यह आंदोलन पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रतीक था।
देशभर में जनता ने अभूतपूर्व एकता और बलिदान का परिचय दिया।
6. क्रांतिकारी आंदोलन का योगदान
जहाँ गांधीजी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, वहीं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति का मार्ग चुना।
उनका उद्देश्य था — भारत को विदेशी शासन से तुरंत मुक्त कराना।
भगत सिंह का नारा “इंकलाब ज़िंदाबाद” आज भी युवाओं के दिलों में जोश भर देता है।
क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता संघर्ष में नई ऊर्जा और साहस का संचार किया।
7. महिलाओं की भूमिका
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने भी अग्रणी भूमिका निभाई।
सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, रानी लक्ष्मीबाई, कस्तूरबा गांधी जैसी वीरांगनाओं ने देश की स्वतंत्रता के लिए अद्भुत योगदान दिया।
उन्होंने जेलों में अत्याचार सहे, सत्याग्रह में भाग लिया और नेतृत्व की भूमिका निभाई।
8. साम्प्रदायिक राजनीति और विभाजन
1940 के दशक में स्वतंत्रता संग्राम के साथ-साथ हिंदू-मुस्लिम विभाजन की राजनीति तेज हुई।
मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग उठाई।
अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन यह स्वतंत्रता विभाजन की त्रासदी के साथ आई।
देश दो भागों में बंट गया — भारत और पाकिस्तान।
9. स्वतंत्रता के परिणाम और महत्व
स्वतंत्रता प्राप्ति केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं थी, बल्कि यह भारत की आत्मा की पुनः स्थापना थी।
स्वतंत्रता ने भारतीयों में लोकतंत्र, समानता, और सामाजिक न्याय की भावना को जन्म दिया।
भारत ने 1950 में संविधान लागू कर एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष, और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की।
10. निष्कर्ष
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम केवल राजनीतिक आज़ादी का आंदोलन नहीं था, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक था।
1857 की क्रांति से लेकर 1947 की आज़ादी तक भारतीयों ने त्याग, बलिदान, और एकता का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया, जो विश्व इतिहास में दुर्लभ है।
आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, हमें उन लाखों ज्ञात-अज्ञात नायकों को नमन करना चाहिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी का उपहार दिया।